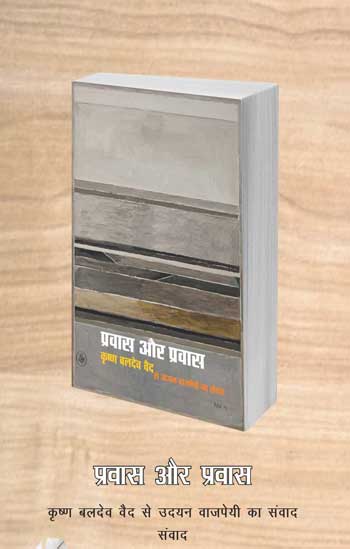
29-Dec-2019 12:00 AM
5321

‘सारी मुहब्बत तो मुझे रूप (फाॅर्म) से थी। मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि उसमें सन्देश क्या है, या उसकी सामाजिक प्रासंगिकता क्या होनी चाहिए या लेखक की सामाजिक प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए।’
शम्सुर्रहमान फ़ारुक़ी
भाषाएँ, हर तरह की दीवारों में रोशनदान, खिड़कियाँ और दरवाज़े खोल देती हैं। साहित्य को रच रही भाषा का स्वप्न, हमेशा ही साहित्य को उसके होने के उदात्त का अनुभव कराना रहता होगा। कोई भाषा अपने औपचारिक बर्ताव को, निर्धारित पद्धतियों में आवृत्ति को, प्रचलित रूपाकारों में ही प्रकट होने की विवशता को कब तक बर्दाश्त कर सकती है। लेखकों के स्वप्न से ज़्यादा बड़े और अर्थगर्भी स्वप्न भाषा के होते होंगे। भाषा लेखक के ऊपर ही निर्भर नहीं होती लेकिन लेखक सिफऱ् भाषा पर निर्भर होता है। भाषाएँ चाहती हैं कि उन्हें उनके तय प्रारूपों से भिन्न भी बरतने का जोखिम उठाया जाए। वे किन्हीं विधाओं में निरन्तर प्रतिकृत होने के अभिशाप के विरुद्ध भी कल्पना करती होंगी। उन्हें अपनी संरचना, अपने तिलिस्म, अपनी आवाजाही के अकल्पनीय का स्वप्न भी उद्वेलित करता होगा। उनके माध्यम से जिसे साहित्य रूप में रचा जाता है, उसके प्रति भी उनकी कोई आकांक्षा रहती होगी। हो सकता है, वे अपने को तरह-तरह से बरतने की सुघड़ता के बारे में सोचकर, बरतने वाले लेखक के प्रति आश्वस्त भी होती हों !
भाषा पर ही टिका हुआ लेखक, क्या भाषा के इन स्वप्नों के बारे में सोचता है ?
हम जो व्यक्त कर रहे हैं, वह उस भाषा की महती कृपा से कर पा रहे हैं जिसकी आकांक्षा को लेकर हमारे मन में अत्यल्प ही विचार आता है। लेखन एकतरफ़ा घटित नहीं हो सकता। लेखक अपने व्यक्त के लिए व्याकुल हो और जिसके सहारे उसकी व्याकुलता चरितार्थ हो सकेगी, उसे भूल जाए, सम्भव नहीं लगता। इस असम्भावित के लिए लेखन में अनुकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। किसी को लेखक बनना है तो कुछ महान हो चुके लेखकों की पद्धति और विषय अनुरूप लिखने से भी यह काम आसानी-से हो जाएगा, यह चलन में है। सिफऱ् विषय के चुनाव और किसी अनुकरण से लेखन कर्म पूर्ण नहीं हो सकता।
किसी भी रचना के लिए बाहर को जितना ज़्यादा जवाबदेह बनाया जाएगा, रचना उतनी ही बाहरी और बेगानी बनकर रह जायेगी। उसकी आन्तरिक शक्ति को पहचानकर, उसे रचना होता है। उसकी कला, उसके मूल्य, उसमें अन्तर्निहित सृजनात्मक आकांक्षा के माध्यम से ही उसके आत्मसम्मान की प्रतिष्ठा की जा सकती है।
उपन्यासकार का सफ़रनामा किताब उर्दू के मशहूर कथालेखक, आलोचक और सम्पादक शम्सुर्रहमान फ़ारुक़ी से समास सम्पादक के संवाद की निर्मिति है। फ़ारुक़ी साहब जैसा कि संवादी बताते हैं ‘साहित्य में कलात्मक मूल्यों’ को प्रतिष्ठित करने के विरल घटित अध्यवसाय में जीवन भर संलग्न रहे जबकि हमारा समय ग़ैर साहित्यिक मूल्यों के आरोपण और कतिपय काल्पनिक मूल्यों का पक्षधर बना रहा। आलोचना में बहुप्रचलित समाजशास्त्रीय पद्धति इसका साक्ष्य है।
छोटी उम्र में ही साहित्यिक दुनिया से सक्रिय रिश्ता फ़ारुक़ी साहब का बन पड़ा। आठवीं कक्षा में पढ़ते समय उन्होंने हस्लिखित ‘गुलिस्तान’ पत्रिका निकाली; ग्यारहवीं, बारहवीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान कुछ कहानियाँ और एक उपन्यास लिखा। वे पढ़ते भी बहुत थे। उस दौर के लोकप्रिय लेखकों राजेन्द्र सिंह बेदी, इस्मत चुगतई, कृष्ण चन्दर और कुरर्तुल हैदर को उन्होंने पढ़ा। कुछ पठित उपन्यासों के हवाले से उन्होंने अपनी पाठकीय निराशा के बारे में बताया है। दरअसल, ट्रेन टू पाकिस्तान, फूल सुर्ख हैं, पेशावर एक्सप्रेस, जब खेत जागे, और इंसान मर गया जैसे अफ़सानों को ‘पढ़कर यह लग रहा है कि लेखक उसे खुद नहीं सह रहा है। वह तुम्हें बता रहा है कि देखो, यह हो गया। वह उस दर्द से इतना दूर है कि न तो वह उसमें शरीक है न वह जानता है कि शरीक होने वालों पर क्या गुज़र रही है।’
शेक्सपियर को पढ़कर फ़ारुक़ी साहब ने साहित्य की वास्तविक शक्ति को महसूस किया, उन्हें अपने लेखन का मार्ग समझ आया जो तरक्की पसन्दों और कट्टरपन से सर्वथा अलग था। इसीलिये शेक्सपियर को अपनी जि़न्दगी की सबसे बड़ी खोज उन्होंने माना है। थाॅमस हार्डी को वे दूसरी बड़ी खोज बताते हैंः ‘जिसने मेरे अन्तस को समृद्ध किया।’
साहित्य में कलात्मक मूल्यों की निरन्तर अल्पता को महसूस करते हुए उन्होंने अपनी आकांक्षा को चरितार्थ करते हुए ‘शबखून’ पत्रिका निकाली। यह उनके जीवन का एक साहित्यकार के रूप में अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी काम साबित हुआ। उनकी शख्सियत में शबखून के प्रकाशन की शै झलकती है। जिस दौर में पत्रिकाओं के प्रकाशन का एक पैटर्न ही चल रहा हो, कुछ उदार और नितान्त साहित्यिक मूल्यों पर आग्रह करती पत्रिका का निकालना दुष्कर कर्म है। आर्थिक चुनौतियाँ तो अलग ही हैं। फ़ारुक़ी साहब ने ‘शहराज़ाद’ नाम से न केवल अनुवाद किए बल्कि ‘जावेद जमील’ नाम से खुद ही कहानी और अन्य नामों से लेख वगैरह लिखकर पत्रिका का स्तर और अंक की समग्रता को कायम रखा। शबखून के लिए उनकी पत्नी ज़मीला ने यदि आर्थिक उत्तरदायित्त्व का सहर्ष निर्वाह किया तो फ़ारुक़ी साहब ने अंक वांछित लेखन सामग्री का। फ़ारुक़ी साहब ने अपने नाम से जितना मूल्यवान लेखन किया, दूसरे नामों से, उससे कम नहीं। ऐसी पत्रिकाएँ दो-एक ही होती हैं जिनके निकालने की वजह गहरी कलात्मक-साहित्यिक हो और जिसके निकालने का उद्यम सम्पादक को अन्य नामों से वांछित लेखन कर पूर्ण करना पड़े। उनकी इस जि़द और महत्त्वाकांक्षा ने उन्हें भरापूरा ही बनाया, इसीलिये वे कह पाते हैंः ‘यह पत्रिका न होती तो फ़ारुक़ी साहब भी न होते।’ इस पत्रिका की उल्लेखनीयता यह भी है कि इसका कोई विशेषांक नहीं निकला तथा कुछ मूल्यों के लिए यह सदा प्रतिबद्ध रहीः ‘लेखक को हमेशा अपने दिल की बात कहने की आज़ादी मिलना चाहिए, उसे किसी राजनैतिक कार्यक्रम का मातहत नहीं होना चाहिए, प्रयोगधर्मिता को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेखक पर ग़ैरलेखकीय जि़म्मेदारी नहीं ठोकी जाना चाहिए।’
दूसरे नाम से लिखना केवल शबखून की विवशता ही नहीं थी। फ़ारुक़ी साहब ने गल्प की कला और उसके यकीन में आस्था को निरन्तरता देने के लिए, दूसरे नामों से अफ़साने लिखे। उन्होंने ग़ालिब के जीवन पर ‘ग़ालिब अफ़साना’ लिखा लेकिन उसे विश्वसनीय बनाने के लिए लेखक का नाम बेनी माधव रुसवा रखा जिसकी भाषा ग़ालिब के समय की पुरानी उर्दू रखी। अपनी कल्पना से ग़ालिब-रुसवा के संवाद और रुसवा के शेर लिखे। इस वक़्त के और भी पहले का किस्सा लिखने की कल्पना करने पर रुसवा को रुखसत कर उमर शेख मिजऱ्ा के नाम से ‘आफ़ताबे ज़मीं’ कहानी लिखी।
फ़ारुक़ी साहब का उपन्यास ‘कई चाँद थे सरे आसमाँ’ पिछले बीस-तीस बरस की हिन्दी-उर्दू के कथा लेखन की एक बड़ी उपलब्धि है। उपन्यास के एकदम नए रूपाकार, उसके समय का विस्तार, वर्णन का वैचित्र्य और कल्पना व इतिहास का रसोन्मुख मेल उसे न केवल विस्मयपूर्ण पठनीयता प्रदान करते हैं बल्कि एक भिन्न औपन्यासिक आस्वाद भी देते हैं। सलीम जाफ़र के कथात्मक अवदान और दाग़ की अम्मा, वज़ीर खानम के चरित्र के रहस्य को शायरी, प्रेम, जुनून, जि़द के आवेग पर, काव्यात्मक भाषा से एक-एक कथा के सिलसिले को अन्य कथाओं के प्रस्ताव के मानिन्द जिस तरह अतीत और कल्पना में गोताखोरी के साथ प्रतिकृत किया है, वह औपन्यासिक रचाव की भव्यता है। वे खुद ही इस उपन्यास के बारे में बताते हैंः ‘उपन्यास में मैंने इस थीम का प्रवेश कराया कि कला और जि़न्दगी का परस्पर विनिमय है, कला जीवन बन सकती है, जीवन कला। जब ऐसा होता है, चमत्कार हो जाता है।’
उपन्यास को लेकर फ़ारुक़ी साहब के विचार मूलतः औपन्यासिक कला के बारे में ही हैं। उपन्यास में ‘वर्णन’ को वे अत्यंत ज़रूरी मानते हैं, ‘कई चाँद थे सरे आसमाँ’ इसका साक्ष्य है। फ़ारुक़ी साहब ने ए.एस. बायट के हवाले से वर्णनात्मकता को स्पष्ट किया है; वर्णन की शक्ति से ही पाठक के मन में दृश्य चरितार्थ हो पाते हैं।
कुछ अप्रचलित अनोखी बातें भी इस संवाद से पता चलती हैं। मुसहफ़ी उस्ताद थे और आतश शागिर्द। आतश के लेखन तेवर से मुसहफ़ी इतने प्रभावित थे कि वे उसी रंग में लिखने लगे, उनका सातवाँ और आठवाँ दीवान इसका प्रमाण है। इसी तरह ग़ालिब और दाग़ के बारे में कुछ सूक्ष्म बातें भी इस संवाद में आती हैं जिनसे दाग़ की काबिलियत, ग़ालिब में अँग्रेज़ी राज के स्थायित्व की समझ का न होना तथा उनकी जानबूझकर की गई अनदेखी के साथ ही अकबर इलाहाबादी के हवाले से सामुदायिक जीवन में आए बदलाव भी बयाँ हैं। अमीर मीनाई द्वारा अपने नाई की दरयाफ्त पर यात्राओं के दौरान उसके लिए दीवान लिखना भी दिलचस्प किस्सा है जो रचनाशीलता, उदारता, दूसरे का सम्मान और मौलिकता जैसे अभिप्रायों को प्रकट करता है।
लेखन में सामाजिक प्रतिबद्धता की अपेक्षा के बरक्स फ़ारुक़ी साहब ज़ोज़ेफ ब्रोड्स्की की उक्ति पर आग्रह प्रकट करते हैंः ‘लेखक की सबसे बड़ी सामाजिक जि़म्मेदारी ये है कि वह अच्छा लिखे।’ नए पुराने के द्वन्द्व को उन्होंने संकट नहीं माना, पुराने को नया नकारता नहीं है, नया पुराने के ऊपर टिप्पणी होता है। आलोचनात्मक उद्यम पर भी उनकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति हैः ‘सब पर नहीं लिखा, जिस पर मन आया, लिखा। मैं किसी पर लिखने के लिए बाध्य नहीं हूँ।’
संवाद में प्रश्नों का काम पूछने के भाव से मुक्त होकर संवाद को नैरन्तर्य देना, हो जाता है।
इस किताब में संवाद की सम्पन्नता के ठीक बाद फ़ारुक़ी साहब का एक निबन्ध ‘फि़क्शन की सच्चाइयाँ’ शामिल है। शीर्षक से ही यह भाव स्पष्ट है कि हमारे यहाँ फिक्शन अर्थात् उपन्यास या अफ़साना के अर्थ संशय पर अलग-अलग दृष्टियाँ मौजूद हैं। आम तौर पर किन्हीं आग्रहों के आधार पर उसे एकतरफ़ा परिभाषित कर दिया जाता है जैसे हक़ीक़त बयान, आदि। फ़ारुक़ी साहब ने किसी रचना के फि़क्शन हो पाने की शर्त पर बहुत ठोस विचार दिया है। उनका मानना है कि फि़क्शन हक़ीक़त के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। इसे दूसरे शब्दों में झूठ पर आधारित भी कहा जा सकता है। हक़ीक़त होने का दावा करने वालों से उनका प्रश्न भी हैः ‘फिर ऐसी तहरीर को फि़क्शन कहने का औचित्य क्या है ?’ उनके विचार से फि़क्शन कल्पना की निर्मिति है जिसमें अन्य तत्त्वों का समावेश सहायक तो हो सकता है लेकिन आधार नहीं हो सकता। उनका विचार है कि जो भी अफ़साने किसी ने गढ़े हैं, वे दरअसल हमारे ख्वाब हैं। बस होता इतना भर है कि अफ़सानानिगार हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम उसके वाकये को सच मानें।
फ़ारुक़ी साहब प्रेमचंद, इयन वाट और लूकाच जैसे लेखकों के हवाले से फि़क्शन के पैगाम या मकसद को फि़क्शन के लिए नुकसानदेह मानते हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में फि़क्शन एक तरह से फै़सला देने वाला बन जाता है जबकि उसका असली रचनात्मक उत्कर्ष यही हो सकना चाहिए कि उसे पढ़ने वाला, अपने फै़सले खुद ले सके। रोज़मर्रा के घटित और फि़क्शन में वर्णित की प्रभावोत्पादकता की तुलना करते हुए फ़ारुक़ी साहब ने फ़्लोबे के उपन्यास ‘मादाम बोवरी’ में मादाम बोवरी की ख़ुदकुशी और मारिओ वार्गास लिओसा के उपन्यास ‘द बेड गर्ल’ में बुरी लड़की की उच्छृंखलता के हवाले से यह स्पष्ट किया है कि सामने घटित से ज़्यादा हम फि़क्शन के घटित से अपना तादात्म्य स्थापित कर जाते हैं, उसे पढ़कर छटपटाते हैं।
फि़क्शन के बारे में इस निबंध से कुछ बातें स्पष्ट हो पाती हैंः यह जानते हुए भी कि फि़क्शन में जो पढ़ रहे हैं वह फ़जऱ्ी है, हम उसे हक़ीक़त मानते हैं। फि़क्शन में घटित हमारे लिए अतीत नहीं होता, वह हर बार पढ़ते हुए नैरन्तर्य का बोध कराता है। अफ़सानानिगार अफ़साने के आंतरिक सौंदर्य का साधक होता है।
फ़ारुक़ी साहब के निजी जीवन के कुछ प्रसंगों और लेखन में उनके मार्ग तथा उसके निर्वाह के सतत अध्यवसाय से हमें साहित्य में मौलिक रास्ते का जि़द भरा लेकिन आनन्दपूर्ण संघर्ष मिलता है। एक लेखक बनने का अपारंपरिक ढंग, अफ़साने के समय से उसकी भाषा के साम्य हेतु लेखक और भाषा को गढ़ने की कवायद, आलोचनात्मक उद्यम के निर्वाह में अफ़साने को स्थगित करने का नैतिक लेखकीय जोखिम तथा फि़क्शन की मुकम्मल समझ देने के अर्थ में इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। फ़ारुक़ी साहब से हुए सम्वाद को पढ़कर, उन्हें और उनके लेखन को जानने की उत्सुकता ज़रूर पैदा हो सकेगी। दाग़ के एक शेर को उन्होंने ही उद्धृत किया है ः
ऐ दाग़ उसी शोख़ के मज़मून भरे हैं
जिसने मेरे अशआर को देखा, उसे देखा।
उपन्यासकार का सफ़रनामा (शम्सुर्रहमान फ़ारुक़ी से उदयन वाजपेयी का संवाद)
रज़ा पुस्तक माला, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली
प्रकाशन वर्षः 2018 , कीमतः 199 रुपये