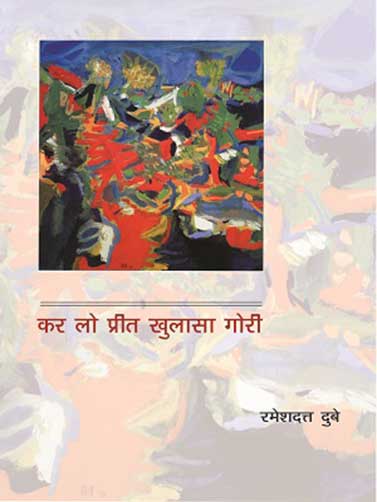
13-Sep-2020 12:00 AM
12033
जिसे हम हिंदी – उर्दू क्षेत्र कहते हैं उस की जान लोकभाषाएँ और उन का लोक – साहित्य है | नागार्जुन ने भारतेंदु पर लिखी अपनी कविता में यों ही नहीं लिखा है कि “हिंदी की असली रीढ़ है गँवारू बोली, यह उत्तम भावना तुम्हीं ने हम में घोली |” एक ज़माने में हिंदी में लोक – साहित्य पर ख़ूब काम हुआ था | हिंदी के श्रेष्ठ लेखकों – कवियों ने लोक – साहित्य का अध्ययन और संकलन किया था | यहाँ द्विवेदीयुगीन कवि रामनरेश त्रिपाठी और बाद के कवि रामइकबाल सिंह राकेश एवं लेखक देवेंद्र सत्यार्थी को याद किया जा सकता है | डा. सत्येंद्र, प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक उदयनारायण तिवारी और कृष्णदेव उपाध्याय का काम भी स्मरणीय है | पर आगे चलकर लोक – साहित्य के अध्ययन की परंपरा क्षीण होती हुई दिखाई देती है | यह सुखद है कि रज़ा फाउंडेशन की रज़ा पुस्तकमाला के अंतर्गत बुंदेली में अत्यंत लोकप्रिय और महाकवि माने जाने वाले ईसुरी का मूल पाठ के साथ खड़ी बोली में रमेशदत्त दुबे द्वारा किया गया रूपांतरण ‘कर लो प्रीत खुलासा गोरी’ प्रकाशित हुआ है |
ईसुरी प्रेम, सौंदर्य और काम – चेतना की अकुंठ अभिव्यक्ति के जबरदस्त कवि हैं | उन का जन्म 1824 ई. में झाँसी के मेढ़की गाँव में हुआ था | उन्होंने जिस काव्य – रूप को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया उसे ‘फाग’ कहते हैं | महज चार या छह पंक्तियों में गहरी से गहरी अनुभूति का मार्मिक अंकन इन की विशेषता है | प्रेम, सौंदर्य और काम – चेतना को ले कर एक भोगवादी दृष्टि भी रही है और एक ‘सहृदय’ एवं ‘रसिक’ की संवेदनशील दृष्टि भी | कई बार प्रेम, सौंदर्य और काम – चेतना को ले कर संकोच भाव इतना प्रबल रहा है कि इसे आध्यात्मिक ढाँचे में भी सीमित किया गया है | विद्यापति की कविताओं के प्रसंग में इसी प्रवृत्ति को ले कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा प्रसिद्ध अंश भी याद किया जा सकता है कि “आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं | उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने ‘गीत – गोविंद’ के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी | सूर आदि कृष्ण – भक्तों के शृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं | पता नहीं बाल – लीला के पदों का वे क्या करेंगे |” रमेशदत्त दुबे ने ईसुरी के फागों के अपने रूपांतरण की प्रस्तावना में अत्यंत सहज भाव से प्रेम, सौंदर्य और काम – चेतना को स्वीकार करते हुए लिखा है कि “जीवन का अर्थ सिर्फ़ होने में नहीं, प्रेम में होने में ही रहा है | प्रेम करने की सामर्थ्य मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में न सिर्फ़ चमत्कारी घटना मानी गयी है वरन् जीवन को अर्थ और चरितार्थ करने की शक्ति भी इसी से मिली है | आसक्ति के लिए देह चाहिए | देहवादी होना गहरा प्रेम होना है कामी – लम्पट नहीं | रीतिकाल नारी को ऐसी ही प्रतिष्ठा देने के उपक्रम का युग है |” रमेशदत्त दुबे का यह सूत्र कि “देहवादी होना गहरा प्रेम होना है” अगर लोगों के ध्यान में रहता तो हिंदी के रीतिकालीन साहित्य की इतनी उपेक्षा नहीं हुई होती!
ऊपर यह कहा गया है कि ईसुरी प्रेम, सौंदर्य और काम – चेतना के कवि हैं | उद्दाम आकर्षण, गहन प्रेम और सहज लालसायुक्त काम ईसुरी की फागों में मज्जा की तरह पैवस्त है | लोक जीवन में यह भाव प्रबलता से अभिव्यक्त होता रहा है | इन फागों में कई बार नारी स्वर में बोला गया है जिसे देख कर यह लगता है कि नारी स्वर में भी प्रेम, सौंदर्य और काम – चेतना की अभिव्यक्ति की जा सकती है ! आज भी भारतीय समाज में यदि स्त्री प्रेम, सौंदर्य और काम – चेतना की अभिव्यक्ति करती है तो उसे ‘चरित्रहीनता’ का प्रमाणपत्र थमाते हुए सब के लिए ‘उपलब्ध’ मान लिया जाता है | ईसुरी के यहाँ आत्मविश्वास से बोलती नारी का स्वर है | एक फाग में एक स्त्री कहती है :
काजर काय पे दिइये कारे, बारे बलम हमारे
सांज भये ब्याही की बेरां, करें बिछौना न्यारे
जब छू जात अनी जोबन की, थर – थर कंपत बिचारे
का काऊ खों खोर ईसुरी, फूटे करम हमारे |
रमेशदत्त द्वारा इस का किया गया रूपांतरण है :
किसके लिए करूँ
भला मैं
बनाव – शृंगार
पिया हमारे
सन्ध्या होते
सो जाते हैं
तिसपर उनकी न्यारी शैया
धोखे से भी छू जायें
कुचाग्र यदि तो
थर – थर काँपें
इसमें कोई दोष न उनका
मेरा ही दुर्भाग्य
पिया हमारे हैं
अबोध – नादान
या फिर
जुबना धरे ना बांदे राने, ज्वानी में गर्राने
मस्ती छाई इन दोउन पे, टोनन पे सर्राने
फेंके – फेंके फिरें ओढ़नी, अंगिया नईं समानें
मन्सेलू पा जायें जिदना, पकरत हा – हा खानें
जांगन में दब जानें जिदना, राम धरे लो जानें |
इस का भी रमेशदत्त दुबे द्वारा किया गया रूपांतरण प्रस्तुत है :
सारे अवरोधों को नकारता
भरपूर यौवन
मस्ती में
उतार फेंकता है
कंचुकी और ओढ़नी
घायल कर देता है कई को
अपने अग्रभाग को
विकसित करते उरोज द्वय
पूर्ण पुरुष के आगे
निरभिमान समर्पित होते
ऊपर के दो उदाहरणों को देख कर यह नहीं समझना चाहिए कि ईसुरी देह की सीमा में ही क़ैद हैं | दरअसल सहज आकर्षण, उद्दाम लालसा और सूक्ष्म कामानुभूति एवं अश्लीलता का अंतर इतना महीन है कि इस में बहुत सावधानी की ज़रूरत है, नहीं तो इस में कुछ का कुछ होने की संभावना है | देह की खंडित प्रस्तुति यानी भावना और प्रक्रिया से कटी अभिव्यक्ति अश्लीलता है | सहज आकर्षण, उद्दाम लालसा और सूक्ष्म कामानुभूति को ठोस रूप से केवल देह में ही सीमित या सिकोड़ देना अश्लीलता है | महत्त्व अंतस्तल तक पैठी अनुभूति और ठोस देह की सहज स्वीकार वाली स्थिति का है | ईसुरी के ही एक फाग से यह बात शायद स्पष्ट हो :
नईयां रजऊ काऊ के घर में, बिरथां कोऊ नें भरमे
सब में हैं और सबसे न्यारी, सब ठोरन में मरमें
को कय अलख – खलक की बातें, लखी न जाये नज़र में
ईसुरी गिरिधर रयें राधा में, राधा रयें गिरिधर में |
बात को और अधिक सहजता से प्रकट करने के लिए इस फाग का रमेशदत्त दुबे द्वारा किया गया रूपांतरण भी नीचे दिया जा रहा है :
प्रेम में ही होती है प्रेमिका
ज्यों राधा में श्याम
श्याम में राधा
मेरी तीन सौ साठ फागों में
उसका नाम
महज़ एक ख्याल है
उसका न कोई पता है
न ठिकाना
सभी जगह है
सब में है
लेकिन न्यारी
वह लौकिक है
मगर विदेही
कहें ईसुरी ––
वह दृष्टि में नहीं
दृष्टि ही वह है |
उपर्युक्त ‘फाग’ और रमेशदत्त दुबे द्वारा किया गया ‘रूपांतरण’ ध्यान से देखने पर ‘रूपांतरण’ की विशिष्टता भी समझ में आती है | रमेशदत्त दुबे के द्वारा ‘फागों’ का ठेठ ‘अनुवाद’ नहीं किया गया है | एक तरह से कहा जा सकता है कि यह ‘रूपांतरण’ ‘पुन:सृजन’ है | लोकभाषा से खड़ी बोली में | एक भाषा से दूसरी भाषा की प्रकृति कितनी भिन्न होती है और एक से दूसरे में किया गया अनुवाद या रूपांतरण कैसे बदल जाता है इस का प्रमाण ऊपर इस पंक्ति ‘जुबना धरे ना बांदे राने, ज्वानी में गर्राने’ से शुरू हो रहे फाग की तीसरी पंक्ति ‘फेंके – फेंके फिरें ओढ़नी, अंगिया नईं समानें’ की भंगिमा को देख कर महसूस किया जा सकता है | ‘फेंके – फेंके फिरें ओढ़नी’ की भंगिमा और ‘उतार फेंकता है कंचुकी और ओढ़नी’ की भंगिमा एक नहीं है | हो भी नहीं सकती है | कहने की ज़रूरत नहीं कि मूल फाग की भंगिमा अपनी विशिष्टता में बेधक है |
‘कर लो प्रीत खुलासा गोरी’ की विशेषता यह भी है कि इस में ‘लोकोक्ति और कहावत’ लेख है | इस लेख में अत्यंत स्पष्ट तरीक़े से उक्ति, लोकोक्ति, कहावत, पहेली, अटका और लटका को सोदाहरण समझाया गया है | इतना ही नहीं लोक -जीवन में पगे – रमे कवि त्रिलोचन से ‘लोक का मतलब’ पर संवाद भी है | त्रिलोचन इस कदर लोक – जीवन में रचे – बसे थे कि उन्हें हिंदी कविता में ‘लोक का निर्देशक’ कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति न होगी | अगर अतिशयोक्ति हो भी जाए तो यह बुरा नहीं क्योंकि अतिशयोक्ति किसी कवि के प्रसंग में नहीं होगी तो कहाँ होगी ? इस के साथ इसी किताब में ‘विहंग’ शीर्षक ललित निबंधनुमा लेख भी है जिसे पढ़ना आह्लादित होना है | ‘कर लो प्रीत खुलासा गोरी’ हमारे लोक – साहित्य की ऐसी बानगी प्रस्तुत करती है जिसे महसूस कर हम गर्वित भी होते हैं और लोक – जीवन एवं साहित्य की ओर प्रेरित भी |