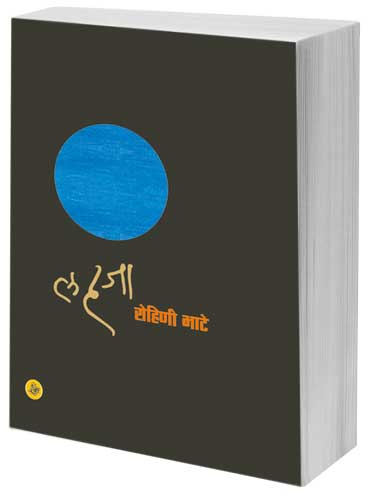
30-Aug-2020 12:00 AM
12374
हिंदी में ललित कलाओं से जुड़ी पुस्तकों का घोर अभाव है | हिंदी में साहित्यिक विषयों से संबद्ध जितनी किताबें छपती हैं उस मात्रा में दूसरी कलाओं से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन नहीं होता | शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत की व्याख्या करने वाली पुस्तकें भी कम ही हैं | इन परिस्थितियों में रज़ा फाउंडेशन की रज़ा पुस्तकमाला के अंर्तगत प्रख्यात कथक – कलाकार रोहिणी भाटे की मराठी में लिखी पुस्तक ‘लहजा’ का हिंदी में प्रकाशन सुखद है | ‘लहजा’ का तात्पर्य लय है | नृत्य की जान लय ही तो है | वैसे भी भी जीवन में लय ही न हो तो फिर जीवन बचेगा ही नहीं | रोहिणी भाटे पचास से अधिक वर्षों से कथक – नृत्य से जुड़ी रहीं | वे न केवल प्रख्यात नृत्यांगना रहीं बल्कि श्रेष्ठ ‘गुरु’ के रूप में भी समादृत रहीं | पुणे में उन की संस्था ‘नृत्यभारती’ कथक के लिए सक्रिय संस्था है जहाँ नई पीढ़ी को इस में शिक्षित – प्रशिक्षित किया जाता है | कथक नृत्य के इतने दीर्घ अनुभव के बाद उन का इस विषय पर लिखना निश्चय ही उन की साधना का उत्तमांश है | हिंदी में इस किताब का अनुवाद स्मिता दात्ये, नीलिमा अध्ये और सुनीता पुरोहित ने किया है |
‘लहजा’ किताब में सात ‘विभाग’ हैं | पहले ‘विभाग’ में दूसरी कलाओं के साथ नृत्य के संबंध को विश्लेषित किया गया है | रोहिणी भाटे चूँकि नृत्य की मर्मज्ञ हैं इसीलिए दूसरी कलाओं की निजता एवं विशिष्टता को भी वे ख़ूब गहराई से व्याख्यायित कर पाती हैं | उदाहरण के लिए नृत्य और साहित्य के संबंध पर उन का विश्लेषण देखा जा सकता है | उन्होंने लिखा है कि “नृत्य, नाट्य और संगीत कलाओं की भाँति साहित्य प्रयोगजीवी कला नहीं है | इस अर्थ में वह कला क्षणजीवी भी नहीं है या यदि साहित्य को दृश्य – श्रव्य कला न मानें, तो यह भी सत्य है कि नाटक, कविता या कथा – कथन आदि ललित साहित्य वाचन – पठन के रूप में वह ‘श्रव्य’ भी हो सकता है और लिखित स्वरूप में वह ‘दृश्य’ भी हो सकता है | चित्र – शिल्प कलाओं की भाँति साहित्य न तो अवकाशनिष्ठ है और न संगीत की भाँति कालनिष्ठ कला है | यह कहते ही स्पष्ट पता चलता है कि ललित साहित्य में काल और अवकाश का सर्वसाक्षी, सर्वगामी व्यवहार दिखायी देता है |” इस उद्धरण में कितनी सूक्ष्मता से इन कलाओं की विशिष्टता निरूपित की गई है ! आगे वे नृत्य और साहित्य के संबंध की विवेचना करती हुई कहती हैं कि “अचूक अर्थ – प्रकटन और अभिव्यक्ति की, बोली – भाषा और तदनुसार भाषा की, साहित्य की क्षमता नृत्य के अंगविक्षेपों, शरीर – भाषा और भाव भाषा के माध्यम में न होने के कारण अर्थ की सुस्पष्टता की खोज में नृत्य को साहित्यिक भाषा और शब्दों के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार शब्दों से परे के अर्थ को स्पर्श करने और कभी – कभी उसे घेर लेने की जो क्षमता शरीर – भाषा में होती है, वह साहित्य को दृग्गोचर अर्थ – प्रतीति देती है |” कहना व्यर्थ है कि इतनी मर्मग्राहिणी दृष्टि हमारे सामने कलाओं की सूक्ष्मता का पटोन्मीलन जगमग रूप में करती है |
दूसरे ‘विभाग’ में कथक के स्वरूप और उस की विशिष्टता पर विचार है | इस का पहला ही लेख है --- कथा कहे सो कथक ! इस में यह विस्तार से बताया गया है कि आरंभिक स्थिति में कथक का आख्यान – कथा से कितना सघन संबंध था, आगे चलकर कैसे आख्यान – कथा का स्वरूप नष्ट हुआ और फिर कैसे कथक ने पूरी तरह नर्तन रूप अपना लिया | इसी क्रम में लेखिका ने एक उप – कथा से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कैसे सीता ने रावण द्वारा ख़ुद के हरे जाने पर भी उसे कोई शाप नहीं दिया | रोहिणी भाटे लिखती हैं कि “जानकी अपने विवाह के उपरांत अयोध्या में आयी | सास – ससुर की सेवा करना उसका नित्य का नियम था | वह आँगन बुहारती, घर के सारे काम करती | एक रात कुछ अधिक देर तक जागरण हुआ, तो उठने में विलम्ब हुआ | आँगन बुहारते हुए सीता को याद आया कि सासु माँ को दातौन देना तो वह भूल ही गयी है | उसने हाथ में पकड़ा झाडू वहीं छोड़ दिया और वह जल्दी – जल्दी में पानी और दातौन लाने चली, तब वहीं पड़ा झाडू उसके गोरे – गोरे पैरों में चुभ गया और उसमें से रक्त निकलने लगा | जानकी चिल्लाई –– ‘जल न गयी ! जल जाय मुई !’ उसका यह क्रोध देखकर तीनों सासुमाँएँ बहुत घबरा गयीं और बोलीं, यह बहू तो बड़ी तेज है | बहुत गुस्सैल है ... कल को यदि हममें से किसी के पाँव दबाते हुए कोई बात हो जाये, तो यह हमें भी श्राप दे देगी | इतना कहकर उन्होंने तत्काल सारी बात श्री राम को बतायी और जानकी से सेवा करवाने से मना कर दिया | राम ठहरे मातृभक्त | बोले, “सेवा न करवाना जैसे कोई उल्टा – सीधा निर्णय न लें | मैं बात को सम्हाल लूँगा |” तब श्री राम ने जानकी को अपनी शपथ देते हुए उससे उसका क्रोध ही माँग लिया | उसे एकदम नर्महृदय बना दिया | इसी कारण जब पंचवटी में सीधे घुसकर रावण ने जानकी का हाथ पकड़कर उसे लक्ष्मणरेखा से बाहर निकाल लिया, उसका अपहरण किया, तब भी जानकी का सतीत्व रावण को श्राप देने और स्वयं की रक्षा करने के लिए निष्फल ठहरा |” यह छोटी – सी कथा कितनी गहरी व्यंजना लिए है उसे सहज ही समझा जा सकता है | जब मंच पर कथक के माध्यम से इस कथा को प्रस्तुत किया जाता होगा तो निश्चय ही इस की अनेक अर्थ छवियाँ प्रकट होती होंगी, हो सकती हैं | इस कथा से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि भारत में शास्त्रीयता के साथ लौकिकता का मेल सदा रहा है | पुस्तक के इसी ‘विभाग’ में कथक और ठुमरी के संबंध को भी स्पष्ट किया गया है | कथक का ‘सिंगार’ से रिश्ता भी यहाँ वर्णित है | अंत में यह बताया गया है कि हर कलाकृति की तरह कथक भी अंततः एक सौंदर्यानुभव ही है |
तीसरे ‘विभाग’ में ‘कथकानुकूल काव्यविलास’ है | यह मूल मराठी पुस्तक में नहीं था | इस में रोहिणी भाटे द्वारा हिंदी में रचे हुए काव्य का नृत्यांकन है | स्वरलिपि भी दी गई है | इस दृष्टि से यह हिंदी के पाठकों के लिए इनाम है |
दूसरे ‘विभाग’ में जहाँ कथक की परंपरा को समझने की कोशिश की गई है वहीं चौथे और पाँचवें ‘विभाग’ में रोहिणी भाटे की अपनी सृजनात्मकता और उन के अपने प्रयोगों से निष्पन्न ज्ञान एवं अनुभव दर्ज़ हैं | स्वभावतः पुस्तक का यह सब से अधिक रोचक, गहन और उदात्त अंश है | इन की एक और विशेषता है कि ये इस प्रकार लिखे गए हैं कि कथक के ‘जानकार’ भी इन से लाभान्वित हो सकते हैं और साधारण पाठक भी कहीं बोझिल शास्त्रीयता का अनुभव नहीं करते | ‘कथक में प्रयोग’ शीर्षक के अंतर्गत रोहिणी भाटे लिखती हैं कि “ठोस रूप से ‘अंग’, ‘भाव’, तथा ‘ताललयांकन’ ये तीन पहलू कथक के ‘नृत्त’ तथा ‘नृत्य’ इन दोनों घटकों के लिए मौलिक महत्त्व रखते हैं | अंग काअर्थ है –– कथक – वाचक सरल रेखाएँ और अंशमात्र वक्राकारों का सन्तुलनपूर्वक ललित मेल, ‘भाव’ पक्ष में अंगोपांग, हस्त, गतिविधियाँ, पैंतरे आदि माध्यमों द्वारा सरल, तथा सूचक भाव एवं अर्थान्तर का प्रकटन और ताल लय पक्ष में लक्षणीय तालबद्धता तथा पदन्यास द्वारा संकीर्ण लयकारी आदि चीजों का अन्तर्भाव होता है | ‘अंग’, ‘भाव’ तथा ‘ताल लयांकन’ इन तीन घटकों का ‘कथक’ के आविष्कार में संतुलित रूप से मेल होना चाहिए | कथक के विशिष्ट स्वरूप का निर्धारण करने के लिए जिस घटक का जिस परिमाण में योगदान आवश्यक महसूस होता है, उसी परिमाण के अनुसार उस घटक का अविष्कार में महत्त्व होना चाहिए | इस प्रमेय के बल, तथा ‘कथा करे सो कथिक कहलावे’, इस कथक नृत्य की पूर्वपरम्परा का सूचन करने वाली व्याख्या के अनुसार कथक के आविष्कार में ‘नृत्त’ पक्ष से ‘नृत्य’ पक्ष का आधिक्य या समानता रखने की आवश्यकता, मेरे विचार से एक गृहीत तथ्य के समान है |” इस उद्धरण में कथक की विशिष्टता का विवेचन करते हुए यह संकेत किया गया है कि उस में कहाँ – कहाँ प्रयोग की संभावनाएँ हैं ?
छठे और सातवें ‘विभाग’ में संस्मरण हैं | जिन गुरुजनों से रोहिणी जी ने शिक्षा ली उन का कृतज्ञ स्मरण छठे विभाग में है | इस में वसन्तराव देशपाण्डे, पं. मोहनराव कल्याणपूरकर, लच्छू महाराज का स्मरण है | सातवें विभाग में पं. मोहनराव कल्याणपूरकर, कलानिधि नारायणन, अशोक केलकर, और अशोक वाजपेयी के रोहिणी भाटे पर लिखे संस्मरण या लेख संकलित हैं | इन संस्मरणों की विशेषता आत्मीयता, मार्मिकता और उदात्तता है | लच्छू महाराज को याद करते हुए उन की विशेषता को उद्घाटित करते हुए लिखा है कि “साथ ही साथ उपर्युक्त साहित्य का नृत्यांकन भी देखने और सीखने को मिला | ‘रात समय रस केलि कियो, और भोर भई उठि मज्जन धाई, या ‘केहि कारण सुन्दर हाथ जल्यों’ जैसी समस्यापूर्ति के काव्यार्थ हों या अभिधा के स्तर पर भी जाँचने वाला काव्यार्थ हो, तो अभिनय कविता के समान्तर चलता था | किन्तु ‘मोहे छेड़ो ना नन्द के सुनहूँ छैल’ या ‘कांसे खेलूँ पिया घर नाहीं’, ‘उठि है घनघोर घटा यह बरसन लागी’ इत्यादी का भावार्थ अभिनीत हुआ करता था, भाव – भावनाओं की उभरती गिरती लय का लहजा पकड़ के जितनी सहूलियत से महाराजजी शृंगार रस की छटाएँ अदा करते थे, उतनी ही सहूलियत से महाराज जी ‘चलत डगर देखो श्यामकर गहिया’ जैसी ठुमरी में ‘डगर’ शब्द को बूझते हुए उर्ध्वगामी प्राणों की उपमा देते हुए व्यथा तथा उदासीनता की भावच्छटाएँ अभिव्यक्त करते थे |” यह उद्धरण हमें यह भी सिखाता है कि साहित्य के माध्यम शब्द, संगीत के माध्यम स्वर और नृत्य के माध्यम शरीर के बीच कितना गहरा जुड़ाव है ! कोई भी श्रेष्ठ नर्तक या नर्तकी अपनी प्रस्तुति में इन तीनों का मंगल विधान उपस्थित करता है, करती है | माध्यम बदल जाने मात्र से कलाओं के बीच दूरी नहीं बढ़ जाती बल्कि एक कला की प्रस्तुति के दौरान दूसरी के आदरसहित प्रकट होने की संभावना और प्रयास ही किसी भी कलात्मक प्रस्तुति को रचनात्मक बनाता है | रोहिणी भाटे ने इसे अपनी नृत्य – साधना में अर्जित किया है | उन की यह पुस्तक इसी का मूर्त रूप है | निश्चय ही यह पुस्तक समस्त हिंदी संसार ही नहीं बल्कि समस्त कला जगत के लिए उपहार है |